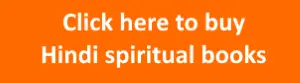बृहदारण्यक उपनिषद

Recommended for you
एक साधारण स्त्री के गर्भ से अवतार क्यों?

क्या आपको पता है भगवान ने वसुदेव और देवकी का पुत्र बनकर ज्....
Click here to know more..सेतुमाधव मंदिर, रामेश्वरम

जानिए भगवान विष्णु रामेश्वरम में सेतुमाधव क्यों कहलाते �....
Click here to know more..विघ्नेश अष्टक स्तोत्र

विघ्नेश्वरं चतुर्बाहुं देवपूज्यं परात्परम्| गणेशं त्वा....
Click here to know more..Excerpt
Excerpt
यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद् भवति भ्रमः ।
तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे ॥
(अष्टावक्रगीता)
आज प्रायः इक्कीस वर्ष होते हैं जब मैंने पहले-पहले बृहदारण्यक उपनिषद्का एक वाक्य सुना था। वह क्षण इस जीवनमें कभी भूल सकूँगा ऐसी आशा नहीं है। उस समय मैं आगरा कालेजका विद्यार्थी था। एक दिन स्थानीय डी० ए० वी० हाई स्कूलमें कोई उत्सव था। एक श्रोताके रूपमें मैं भी वहाँ बैठा था। मेरे श्रद्धेय बन्धु श्रीधर्मेन्द्रनाथजी शास्त्री, तर्कशिरोमणिका भाषण हो रहा था। उन्होंने याज्ञवल्क्य-मैत्रेयीके प्रसङ्गकी चर्चा करते हुए मैत्रेयीके ये शब्द कहे
येनाह नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम् । (२।४।३)
उस समयसे यह वाक्य मेरा पथप्रदीप बन गया। वैराग्यकी जागृतिके लिये इसकी जोड़का कोई दूसरा वाक्य मैंने सम्भवतः अपने जीवनमें नहीं सुना । इससे अधिक मर्मस्पर्शी कोई दूसरी बात कही जा सकती है-ऐसी मेरी कल्पना भी नहीं है।
अस्तु, आज करुणामय प्रभुने उसी उज्ज्वल रत्नकी खानि इस महाग्रन्थको जनताके सामने रखनेका मुझे सौभाग्य दिया है। इसकी महिमाका वर्णन करना सूर्यको दीपक दिखाना है। वस्तुतः उपनिषद् ही तत्त्वज्ञानके आदि स्रोत हैं। उनसे निकलकर ही विविध वाङ्मयके रूपमें विकसित हुई ज्ञान - गङ्गा जीवोंके संसारतापको शमन करती है। बृहदारण्यक उपनिषद् यजुर्वेदकी काण्वी शाखाके वाजसनेयब्राह्मणके अन्तर्गत है । कलेवरकी दृष्टिसे यह समस्त उपनिषदोंकी अपेक्षा बृहत् है तथा अरण्य (वन) में अध्ययन की जानेके कारण इसे आरण्यक कहते हैं। इस प्रकार बृहत् और आरण्यक होनेके कारण इसका नाम बृहदारण्यक हुआ है। यह बात भगवान् भाष्यकारने ग्रन्थके आरम्भमें ही कही है। किन्तु उन्होंने केवल इसकी आकारनिष्ठ बृहत्ताका ही उल्लेख किया है; वार्तिककार श्रीसुरेश्वराचार्य तो अर्थतः भी इसकी बृहत्ता स्वीकार करते हैं
बृहत्त्वाद्ग्रथन्तोऽर्थाच्च बृहदारण्यक मतम्। (सं० वा. ९)
उनकी यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। भाष्यकारने भी जैसा विशद और विवेचनापूर्ण भाष्य बृहदारण्यकपर लिखा है वैसा किसी दूसरे उपनिषद्पर नहीं लिखा। उपनिषद्भाष्योंमें इसे हम उनकी सर्वोत्कृष्ट कृति कह सकते हैं। ___ इस प्रकार सामान्य दृष्टि से विचार करके अब हम संक्षेपमें इसके कुछ प्रधान प्रसङ्गोंका दिग्दर्शन करानेका प्रयत्न करते हैं। ग्रन्थके आरम्भमें अश्वमेध ब्राह्मण है। इसमें यज्ञीय अश्वके अवयवोंमें विराट्के अवयवोंकी दृष्टिका विधान किया गया है। इसके कुछ आगे प्रजापतिके पुत्र देव और असुरोंके विग्रहका वर्णन है। इन्द्रियोंकी दैवी और आसुरी वृत्तियाँ देव और असुररूपसे भी मानी जा सकती हैं। इन्द्रियाँ स्वभावतः बहिर्मुख ही हैं।
पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूः। (क० उ०२।१।१)
अत: सामान्यतः वैषयिक या आसुरी वृत्तियोंकी ही प्रधानता रहती है। इसीसे असुरोंको ज्येष्ठ और देवोंको कनिष्ठ कहा गया है। पुण्य और पापसंस्कारोंके कारण इन दोनों प्रकारकी वृत्तियोंका उत्कर्ष और अपकर्ष होता रहता है। शस्त्रविहित कर्म और उपासनासे दैवी वृत्तियोंका उत्कर्ष होता है और उन्हें छोड़कर स्वेच्छाचार करनेसे आसुरी वृत्तियोंका बल बढ़ जाता है। एक बार देवताओंने उद्गीथके द्वारा असुरोंका पराभव करनेका निश्चय किया। उद्गीथ एक यज्ञकर्मका अङ्ग है, उसके द्वारा उन्होंने आसुरी वृत्तियोंको दबानेका विचार किया। उन्होंने वाक्, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र और त्वक्के अभिमानी देवताओंसे अपने लिये उद्गान करनेको कहा। उन देवताओंमेंसे प्रत्येकने अपने-अपने कर्मद्वारा दैवी वृत्तियोंकी प्रबलताके लिये उद्गान किया; किन्तु उस कर्मका कल्याणमय फल स्वयं ही भोगना चाहा। यह उनका स्वार्थ था। ऋत्विक्का धर्म है कि वह जो कुछ क्रिया करे उसका फल यजमानके लिये ही चाहे। यह स्वार्थ स्वयं ही आसुरी वृत्ति है, इसलिये उनका वह कर्म व्यर्थ हो गया। अन्तमें मुख्यप्राणसे इस कर्मके लिये प्रार्थना की गयी। प्राण परम उदार और सर्वथा अनासक्त है। वह किसी भी विषयको स्वयं नहीं भोगता तथा उसकी कृपासे सारी इन्द्रियाँ अपने विषयोंको भोगती हैं। अन्य सब इन्द्रियाँ सोती भी हैं और जागती भी, किन्तु प्राण सर्वदा सजग रहता है। अतः उसके उद्गान करनेपर असुरोंका दाँव बिलकुल खाली गया और देवताओंकी विजय हुई। इस आख्यायिकासे श्रुति यही बताती है कि पापवृत्तियोंका मूल वस्तुतः स्वार्थ ही है; जबतक हृदयमें स्वार्थका कुछ भी अंश है तबतक जीव भोगासक्तिरूप पापमय बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता और जिसने स्वार्थका सर्वथा त्याग कर दिया है उसपर संसारके किसी भी प्रलोभनका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।
इसके बाद द्वितीय अध्यायके आरम्भमें दृप्तबालाकि गार्ग्य और अजातशत्रुका संवाद है। काशिराज अजातशत्रु तत्त्वज्ञ था और गार्ग्य दृप्त ज्ञानाभिमानी था। उसने जब अजातशत्रुसे कहा कि मैं तुम्हें ब्रह्मका उपदेश करता हूँ तो राजाने उसे उसी क्षण एक सहस्र सुवर्णमुद्रा भेंट किये। इससे श्रुति यह सूचित करती है कि जो सच्चे महानुभाव होते हैं वे दूसरेके दोषकी ओर न देखकर उसका आदर ही करते है। साथ ही इससे ब्रह्मविद्याकी महत्ता भी सूचित की है, जिसकी केवल प्रतिज्ञा करनेपर ही गुणग्राही विद्वान्ने वक्ताके प्रति अपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर दी। इसके पश्चात् गार्ग्यने जिन-जिन आदित्यादिके अभिमानी पुरुषोंमें ब्रह्मत्वका आरोप किया, राजा अजातशत्रुने उन्हें परिच्छिन्न दवमात्र बताकर उनकी उपासनाका भी विशिष्ट फल बताते हुए उन सबका निषेध कर दिया। इस प्रकार अपनी बुद्धिकी गति कुण्ठित हो जानेसे गार्ग्यका अभिमान गलित हो गया और उसने ब्रह्मज्ञानके लिये राजाकी ही शरण ली। राजा उसका हाथ पकड़कर महलके भीतर ले गया और वहाँ सोये हुए एक पुरुषके पास जाकर प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके बृहत्, पाण्डरवास, सोम, राजन् इत्यादि नाम लेकर पुकारा। किन्तु इन नामोंसे पुकारनेपर वह पुरुष नहीं उठा। तब राजाने उसे हाथसे दबाया और वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया। इस प्रसङ्गद्वारा श्रुति यह बताती है कि जितने भी नाम-रूपाभिमानी देव हैं वे वस्तुतः विज्ञानमय आत्मा नहीं है; विज्ञानात्मा नाम-रूपसे परे है। सामान्यतया सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी हृदयदेशमें उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। वस्तुतः वही सबका प्रेरक और सच्चा भोक्ता है, अन्य इन्द्रियाभिमानी देव भी उसीकी विभूतियाँ हैं, उसकी सत्ताके बिना उनकी स्वतन्त्र शक्ति कुछ भी नहीं है। इन्द्रियोंको प्रेरित करनेके कारण ये प्राण हैं किन्तु प्राणोंका भी प्रेरक होनेसे वह प्राणों का प्राण है।
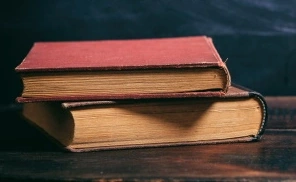
Hindi Topics
आध्यात्मिक ग्रन्थ
Click on any topic to open
- 92 केनोपनिषद
- 91 मुण्डकोपनिषद्
- 90 शाबर मंत्र सागर
- 89 सर्व दर्शन संग्रह
- 88 शक्तिपात दीक्षा
- 87 हवन पद्धति
- 86 शिव गीता - हिन्दी टीका सहित
- 85 काशी की परिक्रमा
- 84 यज्ञ मीमांसा
- 83 दोहावली - तुलसीदास जी - अर्थ सहित
Please wait while the audio list loads..
30
Ganapathy
Shiva
Hanuman
Devi
Vishnu Sahasranama
Mahabharatam
Practical Wisdom
Yoga Vasishta
Vedas
Rituals
Rare Topics
Devi Mahatmyam
Glory of Venkatesha
Shani Mahatmya
Story of Sri Yantra
Rudram Explained
Atharva Sheersha
Sri Suktam
Kathopanishad
Ramayana
Mystique
Mantra Shastra
Bharat Matha
Bhagavatam
Astrology
Temples
Spiritual books
Purana Stories
Festivals
Sages and Saints